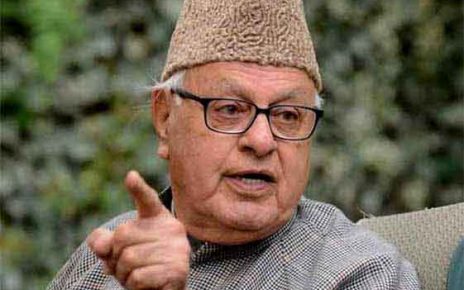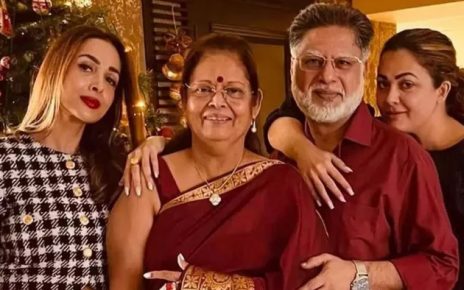- भारत समेत दुनिया के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और अमेरिका के वाशिंगटन व ओरेगन में तेज गर्मी के चलते सैकड़ों लोग मर चुके हैं.
ऐसा माना जा रहा है कि 10 हजार साल में एक बार चलने वाली गर्म हवाओं के कारण यह स्थिति यूरोपीय देशों में बनी है. दिल्ली में भी पारा 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया. इसके उलट न्यूजीलैंड में सर्दी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां बर्फीला तूफान आया हुआ है. इस कारण बर्फ से सड़कें और हवाई अड्डे पट गए हैं.
इस समय न्यूजीलैंड का तापमान 11 से 15 डिग्री रहता है, जो घटकर एक से चार डिग्री नीचे चला गया है. आर्कटिक की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं ने समुद्र की लहरों में ज्वार ला दिया है. ओलावृष्टि के साथ भयंकर बारिश भी हो रही है. वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे हैं कि अंटार्कटिका में जो विशाल हिमखंड टूटा है, वह भी यहां के तापमान में परिवर्तन का कारण हो सकता है, क्योंकि यहां के उत्तरी ध्रुव पर हमेशा माइनस 80 डिग्री तापमान रहता है. ज्यादातर समय ठंडे रहने वाले साइबेरिया के कई इलाकों में लू चल रही है, इन बदलावों के लिए जलवायु परिवर्तन को भी वजह माना जा रहा है.
पोट्सडैम जलवायु प्रभाव शोध संस्थान के वैज्ञानिक-प्राध्यापक एंडर्स लीवरमैन ने धरती के बढ़ते तापमान की वजह से भारत में बारिश पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है. एंडर्स के मुताबिक जितनी बार धरती का पारा वैश्विक तापमान के चलते एक डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ेगा, उतनी ही बार भारत में मानसूनी बारिश 5 प्रतिशत अधिक होगी. मानसूनी बारिश का वास्तविक अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाएगा.
यह अध्ययन अर्थ सिस्टम डायनेमिक्स जर्नल में छपा है. भारत में आमतौर पर बारिश का सीजन जून के महीने से शुरू होता है और सितंबर के अंत तक चलता है. एंडर्स का कहना है कि इस सदी के अंत तक साल दर साल वैश्विक तापमान की वजह से तापमान बढ़ेगा. नतीजतन भारत में मानसूनी बारिश तबाही मचाएगी. इससे ज्यादा बाढ़ आएगी, जिससे लाखों एकड़ में फैली फसलें खराब होंगी.
यह अनुमान वैश्विक तापमान के बढ़ते क्रम के आधार पर लगाया जाता है. पेरिस जलवायु समझौते के अनुबंध के तहत अधिकतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस को तय मानक माना जाता है. इसी से दुनिया के अलग-अलग देशों में मानसूनी या तूफानी बारिश की गणना की जाती है. इस अध्ययन के अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन से भी स्पष्ट हुआ था कि जलवायु परिवर्तन और पानी का अटूट संबंध है. इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया को 2030 तक बाढ़ों की कीमत प्रत्येक वर्ष चुकानी पड़ेगी. इनसे करीब सालाना 15.6 लाख करोड़ की आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है.
साफ है कि वैश्विक तापमान के बढ़ते खतरे ने आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है. दुनिया में कहीं भी एकाएक बारिश, बाढ़, बर्फबारी, फिर सूखे का कहर यही संकेत दे रहे हैं. आंधी, तूफान और फिर एकाएक ज्वालामुखियों के फटने की हैरतअंगेज घटनाएं भी यही संकेत दे रही हैं कि अदृश्य खतरे इर्दगिर्द ही कहीं मंडरा रहे हैं.
समुद्र और अंटार्कटिका जैसे बर्फीले क्षेत्न भी इस बदलाव के संकट से दो-चार हो रहे हैं. दरअसल वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाईऑक्साइड महासागरों में भी अवशोषित होकर गहरे समुद्र में बैठ जाती है. यह वर्षो तक जमा रहती है. पिछली दो शताब्दियों में 525 अरब टन कचरा महासागरों में गया है.